हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाने वाला **विश्व पुस्तक दिवस**आयुर्वेद वालों के लिये पुस्तकों के महत्व और आयुर्वेद ज्ञान के संरक्षण की अहमियत को रेखांकित करता है। यह दिन शेक्सपियर, सर्वंत्स जैसे महान साहित्यकारों की याद दिलाता है, लेकिन भारत की बात करें तो यह हमें **आयुर्वेद** जैसी प्राचीन विद्या के सैकड़ों ग्रंथों की ओर ध्यान खींचता है, जो आज गुमनामी के अंधेरे में खोते जा रहे हैं। आयुर्वेद ज्ञान के संरक्षण की आज अधिक आवश्यकता है।
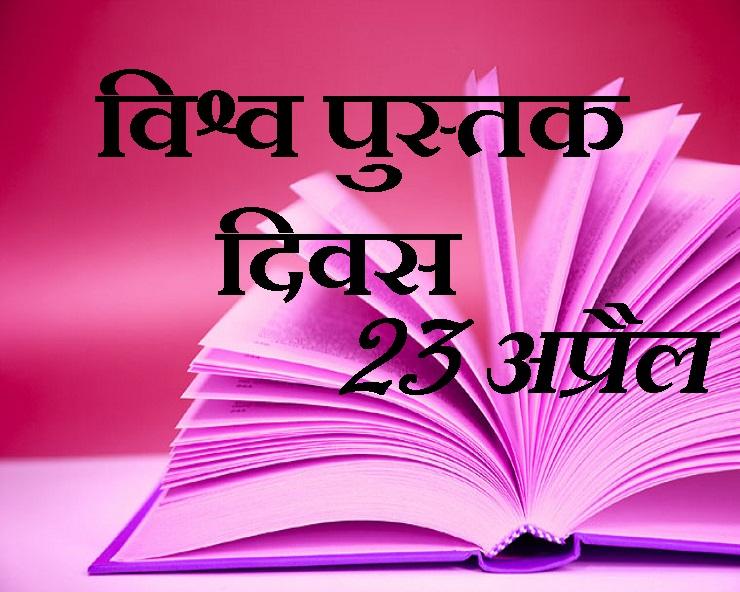
### आयुर्वेद: ज्ञान का सागर, पर पहुंच का संकट
आयुर्वेद ज्ञान दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथों ने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावित किया है। पर आज एक विडंबना है — **इन्हीं ग्रंथों की टीकाएं (भाष्य), संदर्भ ग्रंथ, और क्षेत्रीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी दुर्लभ पुस्तकें लगभग 100 वर्षों से न तो छपी हैं, न ही उनके डिजिटल संस्करण (PDF) उपलब्ध हैं।**
**उदाहरण:**
– **काश्यप संहिता**
(बाल चिकित्सा पर आधारित): इसका अंतिम संस्करण 1920 के दशक में छपा था।
**भेला संहिता:**
चरक और सुश्रुत से भिन्न दृष्टिकोण वाला यह ग्रंथ आज केवल कुछ पुस्तकालयों की धूलभरी अलमारियों में सिमटा है।
**भाव प्रकाश** और **योगरत्नाकर**
इन जैसी टीकाएं: इनके मूल पांडुलिपियां संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रही हैं।
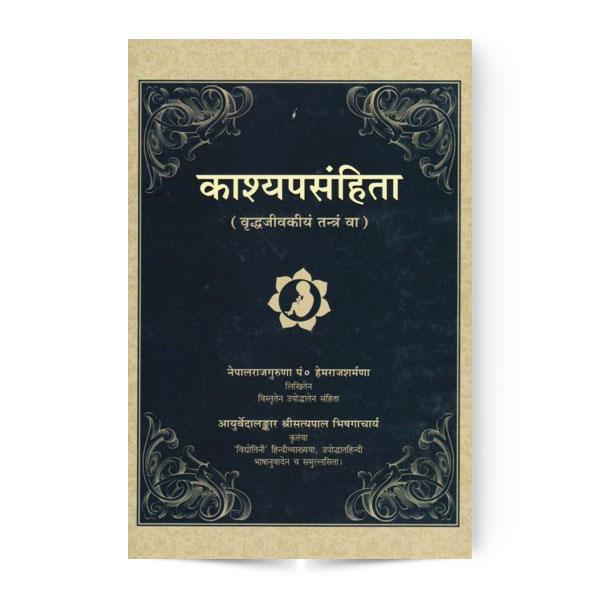
### इंटरनेट युग में आयुर्वेद की चुप्पी
आज डिजिटल दुनिया में हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन 80% से अधिक आयुर्वेद ज्ञान अभी भी **भौतिक पुस्तकों** तक सीमित है। अंग्रेजी और आधुनिक चिकित्सा के लाखों शोध पत्रों के विपरीत, आयुर्वेदिक ग्रंथों की PDFs, ई-लाइब्रेरियां, या ऑनलाइन कोर्सेज न के बराबर हैं। यह अंतर क्यों?
1. **संरक्षण की उपेक्षा:** अधिकांश पांडुलिपियां व्यक्तिगत संग्रह या स्थानीय पुस्तकालयों में बिना उचित देखभाल के पड़ी हैं।
2. **भाषा की बाधा:** संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे इन ग्रंथों के अनुवाद और विश्लेषण का अभाव।
3. **वित्तीय चुनौतियां:** दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलीकरण के लिए फंड और विशेषज्ञों की कमी।
### परिणाम: ज्ञान का क्षरण
**शिक्षा पर प्रभाव:** आयुर्वेद के छात्र आधुनिक शोध से जुड़ने में पिछड़ रहे हैं।
**चिकित्सा अभ्यास:**
पारंपरिक उपचारों की गहरी समझ गायब हो रही है। उदाहरण के लिए, **मधुमेह** के लिए ‘चंद्रप्रभा वटी’ जैसी दवा के मूल सिद्धांत अब कुछ ही ग्रंथों में दर्ज हैं।
**वैश्विक पहचान का नुकसान:**
चीन ने अपनी पारंपरिक चिकित्सा (TCM) को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराकर उसे वैश्विक बनाया, जबकि आयुर्वेद पिछड़ गया।
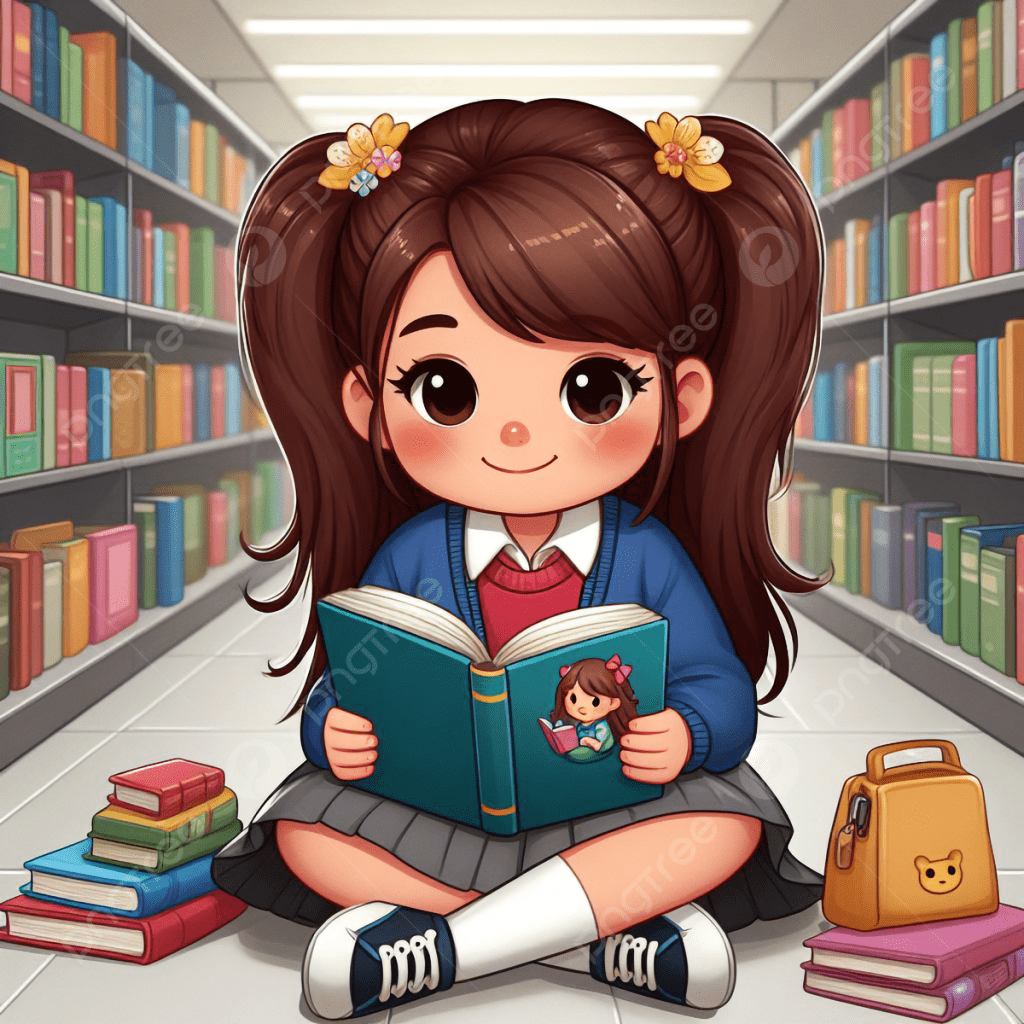
### समाधान: ज्ञान को डिजिटल सूत्र में पिरोना
1. **राष्ट्रीय स्तर की पहल:**
भारत सरकार का ‘नमस्ते योग’ और ‘आयुष पोर्टल’ अच्छे कदम हैं, लेकिन इन्हें ग्रंथों के डिजिटलीकरण से जोड़ा जाए।
2. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:**
बड़े प्रकाशक और टेक कंपनियां AI का उपयोग कर पांडुलिपियों को स्कैन कर सकती हैं।
3. **जनभागीदारी:**
यदि आपके पास कोई पुरानी आयुर्वेदिक पुस्तकें या पांडुलिपियां हों तो भारत सरकार, प्रकाशक या किसी समर्थ वैद्य के संज्ञान में इसे डालें। यदि वह काम की हुई तो इससे सभी का भला होगा।
### **4. केस स्टडी: भेला संहिता और खोई हुई पीढ़ियों का ज्ञान**
भेला संहिता, जिसे “आयुर्वेद का तीसरा स्तंभ” कहा जाता है, चरक और सुश्रुत से अलग नैदानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, इसमें **मानसिक रोगों के इलाज** के लिए योग और आहार के साथ-साथ **ध्वनि चिकित्सा** (मंत्रों का प्रयोग) का विस्तृत वर्णन है। लेकिन 1930 के बाद से इसका कोई नया संस्करण नहीं छपा। आज इसकी मूल पांडुलिपि बंगाल के एक निजी संग्रह में सिमटी है, जहाँ नमी और कीटों से यह नष्ट हो रही है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि **पूरी चिकित्सा पद्धति का अधूरा पाठ** है।
### **5. डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ: सिर्फ स्कैन करना काफी नहीं**
कई लोग सोचते हैं कि पुस्तकों को स्कैन करके PDF बना देना ही काफी है, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों के संदर्भ में यह **पहला कदम मात्र** है। असली चुनौतियाँ हैं:
– **भाषाई जटिलताएँ:** संस्कृत के श्लोकों को समझने के लिए टीकाओं (भाष्य) की आवश्यकता होती है, जो अक्सर अलग-अलग ग्रंथों में बिखरे हैं।
– **संदर्भों का अभाव:** उदाहरण के लिए, “त्रिफला” के फायदे बताने वाले श्लोक में “व्याधि” शब्द आता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा के साथ इसका कोरिलेशन स्पष्ट नहीं हो पाता।
– **मेटाडेटा का अभाव:** पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष, लेखक, या ऐतिहासिक संदर्भ के बिना डिजिटल फाइलें अधूरी रह जाती हैं।
### **6. वैश्विक प्रयासों से सीख: चीन का TCM डिजिटल मॉडल**
चीन ने अपनी पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Chinese Medicine – TCM) को बचाने के लिए जो रणनीति अपनाई, वह आयुर्वेद के लिए प्रेरणादायक हो सकती है:
– **डिजिटल लाइब्रेरियाँ:** 5 लाख से अधिक TCM दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
– **AI और बिग डेटा:** चीन ने AI टूल्स विकसित किए हैं जो पुराने ग्रंथों के आधार पर नए उपचार सुझाते हैं।
– **ग्लोबल पार्टनरशिप:** WHO के साथ मिलकर TCM को इंटरनेशनल मेडिकल कोड सिस्टम (ICD-11) में शामिल किया गया।
भारत के पास आयुर्वेद के लिए **”डिजिटल निदान”** जैसी कोई समग्र योजना नहीं है, जबकि इसकी संभावनाएँ TCM से कहीं अधिक हैं।
### **7. भविष्य की राह: आयुर्वेद 2.0**
आयुर्वेद को डिजिटल युग में प्रासंगिक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
– **ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म:** GitHub जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आयुर्वेदिक ग्रंथों को अपलोड करना, ताकि दुनिया भर के शोधार्थी इसमें योगदान दे सकें।
– **इंटरएक्टिव लर्निंग:** संस्कृत के श्लोकों को एनिमेशन और क्विज़ के साथ समझाने वाले ऐप्स, जैसे “आयुर्वेदिक गेमिफिकेशन”।
– **ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी:** पांडुलिपियों का ओनरशिप और एडिटिंग हिस्ट्री ट्रैक करना, ताकि ज्ञान का मूल स्रोत सुरक्षित रहे।
### **8. पाठकों से आह्वान: ज्ञान के रक्षक बनें**
– **स्कैन और शेयर:** अगर आपके घर में पुरानी आयुर्वेदिक किताबें हैं, तो उन्हें मोबाइल स्कैनर ऐप्स (CamScanner, Adobe Scan) से डिजिटाइज करें।
– **सोशल मीडिया का उपयोग:** #SaveAyurvedicBooks जैसे हैशटैग के साथ जागरूकता फैलाएँ।
– **स्थानीय पुस्तकालयों से जुड़ें:** उन्हें डिजिटलीकरण के लिए प्रेरित करें या स्वयंसेवक बनें।
### **अंतिम पंक्तियाँ: विरासत को अमरता दें**
विश्व पुस्तक दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, एक **जिम्मेदारी** है। आयुर्वेद के ग्रंथों को डिजिटल दुनिया में लाना सिर्फ भारत का नहीं, पूरी मानवता का हित है। जैसे प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिड बनाए, वैसे ही हमें **डिजिटल पिरामिड्स** बनाने होंगे, जो हजारों साल तक ज्ञान को सुरक्षित रखें। याद रखिए, आज का एक क्लिक कल की पीढ़ियों के लिए जीवनरक्षक हो सकता है।
**लेखक की टिप्पणी:**
यह लेख एक “डिजिटल यज्ञ” का आग्रह है, जहाँ हर पाठक एक आहुति बन सकता है। आइए, 23 अप्रैल को केवल किताबें पढ़ने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें अमर बनाने का संकल्प लें।